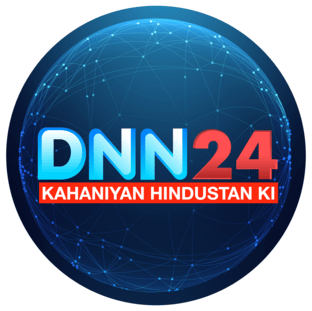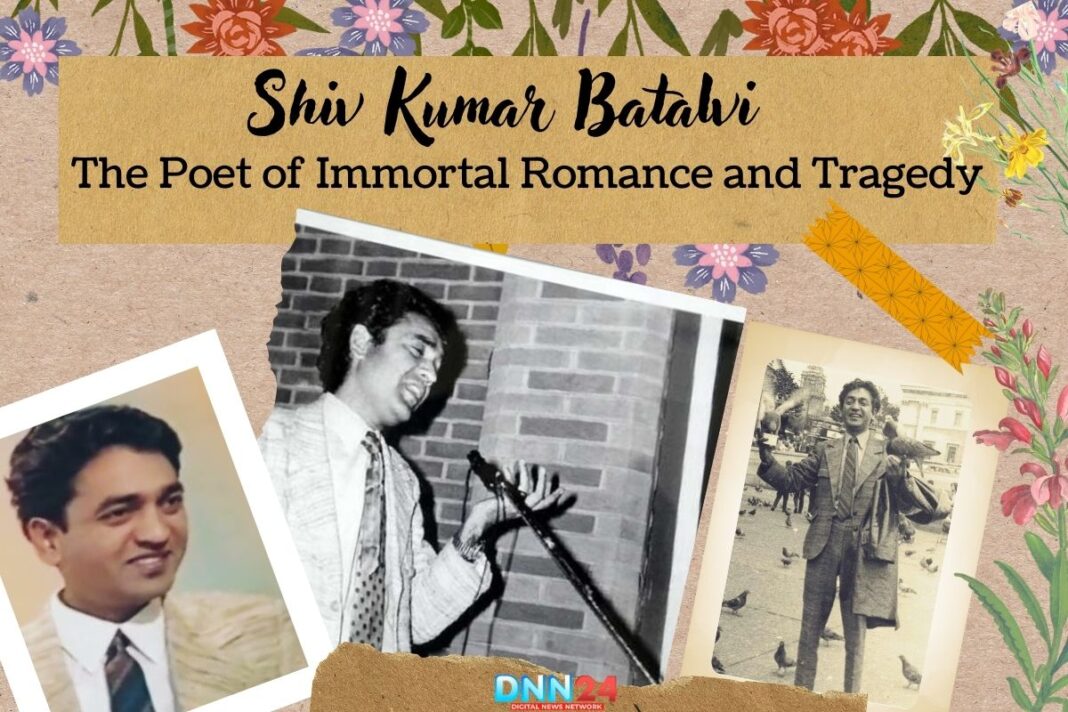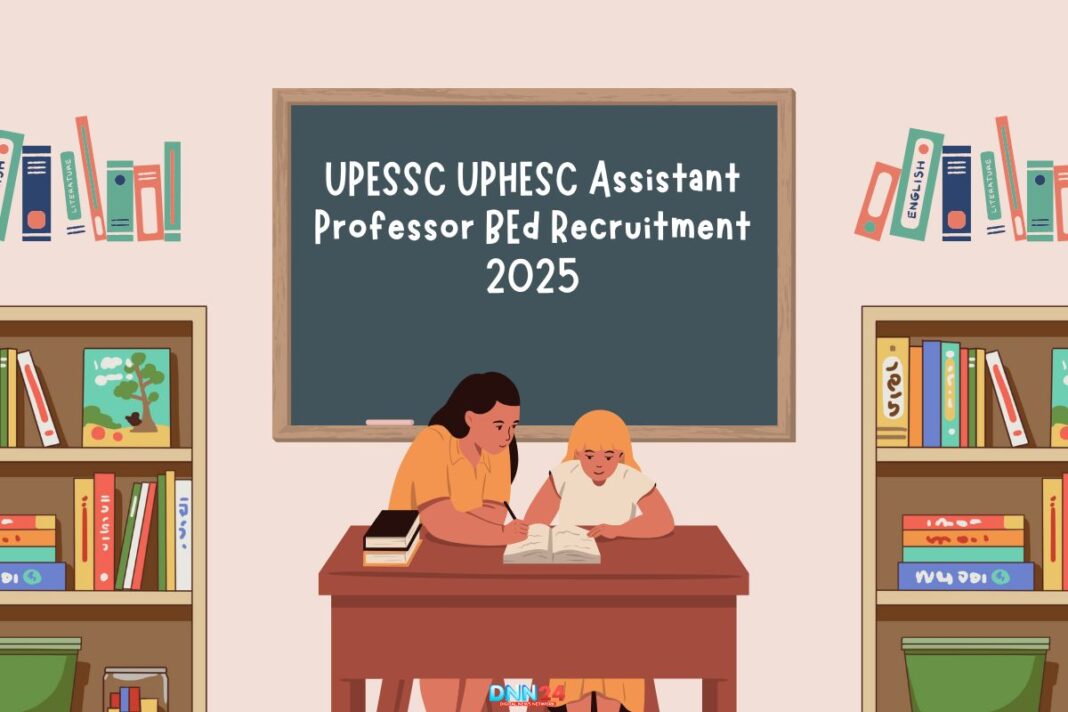शेख़ मुहम्मद इब्राहीम ‘ज़ौक़’,वो नाम जो कभी शाहों की महफ़िलों में गूंजता था, जो कभी दिल्ली की गलियों में मिसाल बना, जो कभी अपने ही हमअस्रों की जलन का शिकार हुआ, और जो आज एक बार फिर उर्दू अदब के फ़लक पर दमकता नज़र आता है।
ज़ौक़, वो शायर जिसे मुग़लिया सल्तनत के आख़िरी दौर में ‘मलिक-उश-शोअरा’ का ख़िताब मिला, और जो ग़ालिब और मोमिन जैसे अज़ीम शायरों के दौर में भी अपनी पहचान बनाए रहा। लेकिन वक़्त के साथ मिज़ाज बदला, ज़माना ग़ालिब परस्ती में ऐसा डूबा कि ज़ौक़ को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। रशीद हसन ख़ां जैसे आलोचक तो यहां तक कह गए कि ग़ालिब और मोमिन के साथ ज़ौक़ का नाम लेना भी गुनाह है।
“अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे
ज़ौक़
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे”
ये वो मिसरा है जो अपने आप में ज़ौक़ की फ़नकारी, दर्दमंदी और ज़बान की लय को बयान करता है। मगर सच्चाई ये है कि ज़ौक़ और ग़ालिब दो जुदा रास्तों के मुसाफ़िर थे। एक ने सादगी और सलीक़े से आम फहम ज़बान में बात की, तो दूसरे ने ख़्याल की ऊंचाइयों को छुआ।
ज़मीनी हक़ीक़तों से शायरी के आसमान तक
ज़ौक़ के वालिद मुहम्मद रमज़ान एक नौ-मुस्लिम खत्री घराने से ताल्लुक रखते थे। घर में न इल्म था, न अदब। मगर क़िस्मत ने ज़ौक़ को हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल के मदरसे तक पहुंचा दिया, जहां उनकी शायरी की बुनियाद रखी गई। तख़ल्लुस ‘ज़ौक़’ भी उस्ताद शौक़ ने ही अता किया।
अदबी सफ़र आगे बढ़ा और जल्द ही वो शाह नसीर जैसे बड़े उस्ताद के शागिर्द हो गए। मगर नसीर की उस्तादी से ज़्यादा उनके हुस्द और तानाकशी ने ज़ौक़ को निखारा। इस बीच दिल्ली के क़िले तक उनकी रसाई हो गई और बहादुर शाह ज़फ़र के वली अहद रहते ही ज़ौक़ को उनका उस्ताद बना दिया गया।
क़सीदे का जादूगर
ज़ौक़ को सिर्फ़ ग़ज़ल का ही नहीं, बल्कि क़सीदे का भी बादशाह माना गया। उनके एक क़सीदे से मुतास्सिर हो कर अकबर शाह सानी ने उन्हें ‘ख़ाक़ानी-ए-हिंद’ का ख़िताब दिया। उन्हें उर्दू का दूसरा सबसे बड़ा क़सीदा निगार तस्लीम किया गया।
उनके क़सीदों में इल्मी रौनक़, ज़बान की सफ़ाई, और फ़न की बारीकियां अपने आप में मिसाल हैं। शाह नसीर तक उनसे रश्क करने लगे, मगर ज़ौक़ ने हमेशा अदब और तहज़ीब का दामन थामे रखा।
दिल्ली से मुहब्बत और सादगी का ज़मीर
ज़ौक़ को न दौलत की हवस थी, न शौहरत का शौक। दिल्ली की गलियों से उन्हें जो मुहब्बत थी, वो इस शेर में छलकती है।
इन दिनों गरचे दकन में है बहुत क़द्र-ए-सुख़न
ज़ौक़
कौन जाए ‘ज़ौक़’ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर
उनकी ज़िंदगी सादगी की मिसाल थी। कई मकान होने के बावजूद एक छोटे से मकान में गुज़ारा किया, और वज़ीफ़ा मिलने पर भी कभी शाही ठाठ नहीं अपनाया।
ज़ौक़ बनाम ग़ालिब: अदबी रक़ाबत या ज़ाती दुश्मनी?
ग़ालिब और ज़ौक़ की अदबी रक़ाबत उर्दू साहित्य का दिलचस्प हिस्सा है। ग़ालिब की तंज़िया चुटकियां और ज़ौक़ का सलीक़ामंद जवाब अदब में लिहाज़ के साथ मज़ाह का बेहतरीन नमूना है। ग़ालिब जब लिखते हैं.
हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता
ग़ालिब
वगरना शहर में ग़ालिब की आबरू क्या है
तो ज़ौक़ इसका जवाब देते हैं.
जिनको दावा-ए-सुख़न है, ये उन्हें दिखला दो
ज़ौक़
देखो इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा
इन दोनों की शायरी में एक तहज़ीब, एक अदबी रस्म-अदा नज़र आती है, जिसमें ख़िलाफ़ भी कला का हिस्सा बन जाता है।
ज़ौक़ की शायरी: सादगी में सलीक़ा और रोज़मर्रा में रवानी
ज़ौक़ ने अपनी शायरी में रोज़मर्रा की ज़बान का इस्तेमाल किया। उनका कलाम कोई गहरा फ़लसफ़ा नहीं देता, मगर दिल तक पहुंचने वाला असर रखता है। उनके शेर आज भी ज़बान-ए-ख़ल्क़ है।
बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो
ज़बान-ए-ख़ल्क को नक़्क़ारा-ए-ख़ुदा समझो
ऐ ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर
आराम से हैं वो जो तकल्लुफ़ नहीं करते
फूल तो दो दिन बहार-ए-जां-फ़िजा दिखला गए
ज़ौक़
हसरत उन ग़ुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए
दीवान की तक़दीर और ग़दर की तबाही
अफ़सोस की बात है कि ज़ौक़ का पूरा कलाम हमारे पास महफ़ूज़ नहीं रहा। वो अपने अशआर को मटकों, तकियों और कपड़ों में छिपा देते थे। इंतेकाल के बाद उनके शागिर्दों ने जो कुछ बचाया, वो भी 1857 की तबाही की भेंट चढ़ गया। उनका दीवान बहुत बाद में, तक़रीबन चालीस साल बाद छपा।
फ़िराक़ और फ़ारूक़ी की नज़र में ज़ौक़
फ़िराक़ गोरखपुरी ने ज़ौक़ की शायरी को ‘पंचायती शायरी’ कहा, लेकिन साथ ही ये भी माना कि उनके यहां कला की अपनी एक अदबी हैसियत है। शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी भी कहते हैं कि ज़ौक़ से मुतास्सिर न होने के बावजूद, उनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है।
बाद रंजिश के गले मिलते हुए रुकता है दिल
अब मुनासिब है यही कुछ मैं बढ़ूं कुछ तू बढ़े
शेख़ मुहम्मद इब्राहीम ‘ज़ौक़’ की शायरी उस दौर की शायरी है जो शाही तर्ज़ की तहज़ीब और आम ज़बान की रवानी को साथ लेकर चलती है। वो न सिर्फ़ एक शायर थे, बल्कि उर्दू ज़बान के जौहर थे। उनकी शायरी में मीर की सोज़ नहीं, मगर एक फ़नकार की सदाक़त ज़रूर नज़र आती है।
ज़ौक़, जिन्हें एक वक़्त कम आंका गया, आज फिर अपने अशआर की वजह से सराहे जा रहे हैं और यही किसी सच्चे शायर की सबसे बड़ी फतह होती है।
ये भी पढ़ें: मजाज़ की आवाज़ बनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहचान
आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।