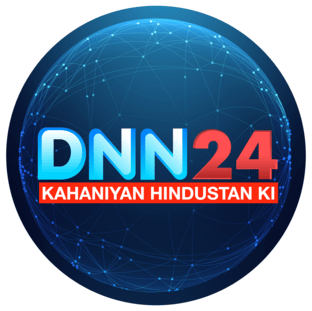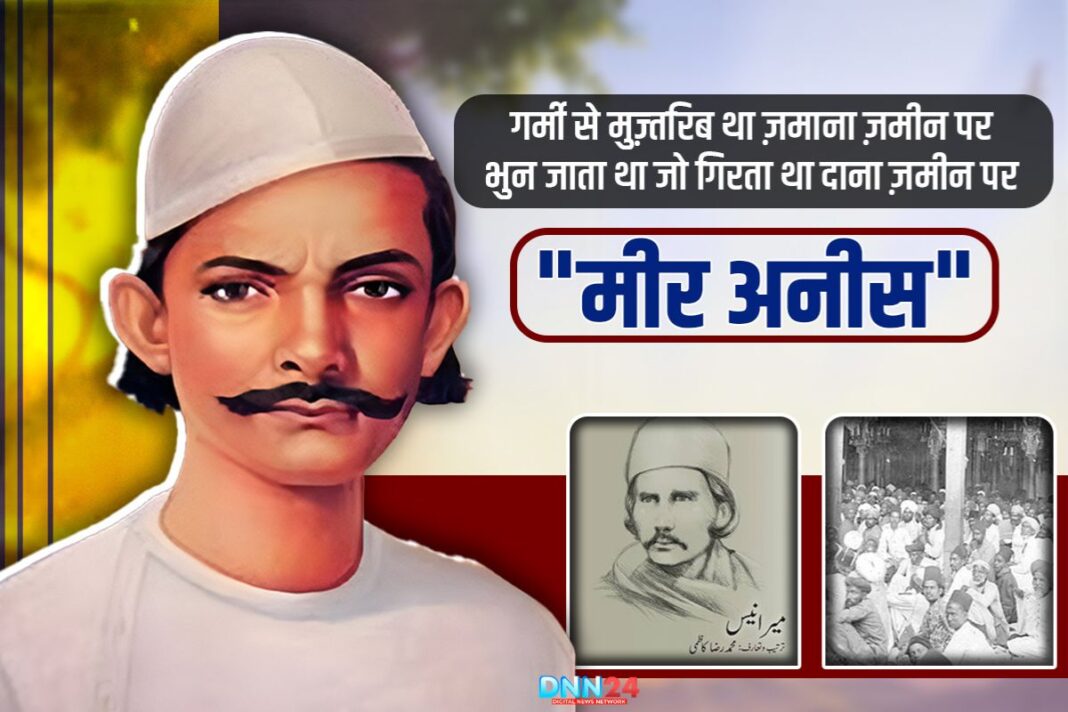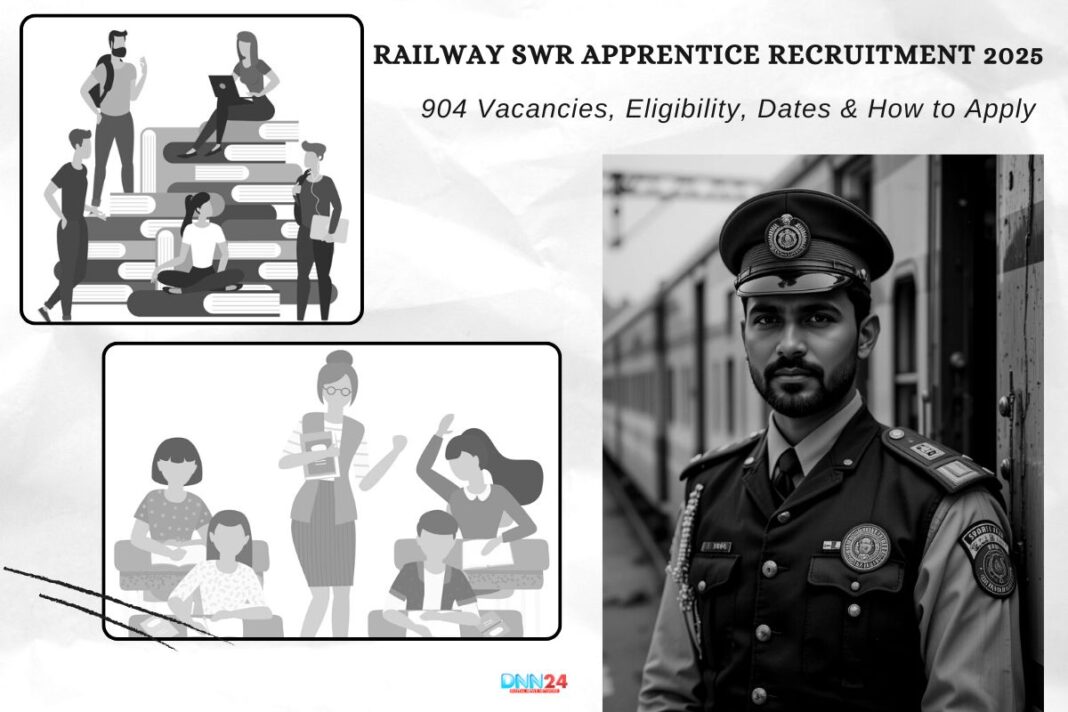उर्दू शायरी की दुनिया में कुछ अज़ीम नाम ऐसे हैं जो अपनी ख़ासियत और कमाल के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। इन्हीं में से एक हैं मीर बब्बर अली अनीस, जिन्होंने शोक काव्य यानी मर्सिया को फ़न के उरूज तक पहुंचाया। उनका नाम आज भी उर्दू अदब में उसी अज़्मत के साथ लिया जाता है, जिस तरह मसनवी में उनके दादा मीर हसन का। अनीस ने इस आम फ़हम ख़्याल को ग़लत साबित कर दिया कि हाई क्लास की शायरी सिर्फ़ ग़ज़ल में ही मुमकिन है। उन्होंने रसाई शायरी (शोक काव्य) को जिस मंज़िल-ए-कमाल तक पहुंचाया, वो अपने आप में बिल्कुल मुख़्तलिफ हैं। आज भी अनीस उर्दू के उन शायरों में से हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा और सराहा जाता है।
पैदाइश और इब्तिदाई सफ़र: एक शायर के ख़ानदान से
मीर बब्बर अली अनीस की पैदाइश 1803 ई. में फ़ैज़ाबाद की ज़मीन पर हुई। उनकी रगों में शायरी थी, क्योंकि उनके वालिद (पिता) मीर मुस्तहसिन ख़लीक़ ख़ुद भी मर्सिया के एक बड़े और नामवर शायर थे। उनके परदादा ज़ाहिक और दादा मीर हसन (जो अपनी मशहूर मसनवी ‘सह्र-उल-बयान’ के मुसन्निफ़ – लेखक – हैं भी अपने वक़्त के अज़ीम शायर थे। ये क़ाबिल-ए-ग़ौर बात है कि इस ख़ानदान के शायरों ने ग़ज़ल की रिवायती राह से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जिस भी विधा को उन्होंने छुआ, उसे कमाल तक पहुंचा दिया। मीर हसन को अगर मसनवी का बादशाह कहा जाए, तो अनीस यक़ीनन मर्सिया के सबसे बड़े शायर क़रार दिए जा सकते हैं।
आशिक़ को देखते हैं दुपट्टे को तान कर
मीर अनीस
देते हैं हम को शर्बत-ए-दीदार छान कर
शायरों के घराने में पैदाइश की वजह से अनीस की तरबियत बचपन से ही शायरी के लिए मौज़ूं थी। कहते हैं कि चार-पांच साल की छोटी सी उम्र में ही, खेल-खेल में उनकी ज़बान से ख़ूबसूरत शे’र निकल जाया करते थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम (प्रारंभिक शिक्षा) फ़ैज़ाबाद में ही हासिल की। रिवायती शिक्षा के साथ-साथ, उन्होंने सिपहगरी (सैन्य कला) में भी महारत हासिल की। हालांकि उनकी गिनती विद्वानों में नहीं की जाती, पर उनकी इल्मी मालूमात को सभी तस्लीम करते हैं। एक बार उन्होंने मिंबर (मंच) से संरचना विज्ञान की रोशनी में सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश को भी साबित कर दिखाया था, जो उनकी गहरी फ़हम को दर्शाता है।
सिवाए ख़ाक के बाक़ी असर निशां से न थे
मीर अनीस
ज़मीं से दब गए दबते जो आसमां से न थे
अनीस को अरबी और फ़ारसी के अलावा हिंदी भाषा से भी ख़ास दिलचस्पी थी। वो तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी के कलाम (रचनाओं) से बख़ूबी वाक़िफ़ थे। कहा जाता है कि बचपन में वो ख़ुद को हिंदू ज़ाहिर कर के एक ब्रहमन विद्वान से हिंदुस्तान के धार्मिक ग्रंथों को समझने जाया करते थे। इसी तरह, जब पड़ोस में किसी की मौत हो जाती थी, तो वह उस घर की औरतों के रोने-पीटने और दुख प्रदर्शन का गहराई से मुताला (अध्ययन) करने जाते थे। ये अनुभव आगे चलकर उनकी मर्सिया निगारी में बहुत काम आए, जिससे उनके मर्सियों में जज़्बात की गहराई और हक़ीक़त की झलक मिलती है।
शायरी का आग़ाज़ और उस्तादी का दौर
अनीस ने बहुत कम उम्र में ही बाक़ायदा शायरी शुरू कर दी थी। जब वो सिर्फ़ नौ साल के थे। फ़ैज़ाबाद में होने वाले मुशायरों में वह ग़ज़लें तो लिखते, लेकिन पढ़ते नहीं थे। तेरह-चौदह साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें उस वक़्त के उस्ताद-ए-शायरी शेख़ इमाम बख़्श नासिख़ की शागिर्दी में दे दिया। नासिख़ जब उनके शे’र देखे, तो दंग रह गए कि इस कम उम्र में लड़का इतने उस्तादाना शे’र कह रहा है। उन्होंने अनीस के कलाम में किसी तरह की इस्लाह (सुधार) को ग़ैर ज़रूरी समझा, अलबत्ता उनका तख़ल्लुस जो पहले ‘हज़ीं’ था, उसे बदलकर ‘अनीस’ कर दिया, जिसका मतलब है ‘साथी’ या ‘दोस्त’।
ख़ाक से है ख़ाक को उल्फ़त तड़पता हूं ‘अनीस’
मीर अनीस
कर्बला के वास्ते मैं कर्बला मेरे लिए
मर्सिया-ख़्वानी का कमाल और अनीस-दबीर की रक़ाबत
अनीस ने मर्सिया कहने के साथ-साथ मर्सिया पढ़ने में भी कमाल हासिल किया था। मुहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि अनीस क़द-ए-आदम आईने के सामने, तन्हाई में घंटों मर्सिया पढ़ने की प्रैक्टिस करते थे। वो अपनी स्थिति, हाव-भाव और हर बात को देखते, और उसमें ख़ुद का सुधार करते थे। कहा जाता है कि सर पर सही ढंग से टोपी रखने में ही कभी-कभी एक घंटा लगा देते थे। ये उनकी कला के प्रति लगन और परफेक्शनिस्ट स्वभाव को ज़ाहिर करता है।
अवध के आख़िरी नवाब ग़ाज़ीउद्दीन हैदर, अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह के ज़माने में अनीस ने मर्सिया गोई (मर्सिया लिखने की कला) में बेपनाह शोहरत हासिल कर ली थी। उनसे पहले दबीर भी मर्सिये कहते थे, लेकिन वो मर्सिया पढ़ने को किसी कला की तरह बरतने के बजाय सीधा-सादा पढ़ने को तरजीह देते थे। उनकी शोहरत उनके कलाम की वजह से थी, जबकि अनीस ने मर्सिया-ख़्वानी (मर्सिया पढ़ने की कला) में भी कमाल पैदा कर लिया था।
शोहरत से मुफ़्लिसी तक: वक़्त का बदलाव
उस ज़माने में अनीस की शोहरत का ये हाल था कि अमीर, नामवर शहज़ादे और आला ख़ानदान के नवाबज़ादे उनके घर पर जमा होते और नज़राने पेश करते। इस तरह उनकी आमदनी घर बैठे हज़ारों तक पहुंच जाती थी, लेकिन इस फ़राग़त का ज़माना (खुशहाली का दौर) मुख़्तसर रहा। 1856 ई. में अंग्रेज़ों ने अवध पर क़ब्ज़ा कर लिया। लखनऊ की ख़ुशहाली रुख़सत हो गई । घर बैठे आजीविका पहुंचने का सिलसिला बंद हो गया, और अनीस दूसरे शहरों में मर्सिया-ख़्वानी के लिए जाने पर मजबूर हो गए। उन्होंने अज़ीमाबाद (पटना), बनारस, इलाहाबाद और हैदराबाद में मजलिसें पढ़ीं, जिसका असर ये हुआ कि दूर-दूर के लोग उनके कलाम और कमाल से वाक़िफ़ होकर उसके प्रशंसक बन गए।
छाए फूलों से भी सय्याद तो आबाद न हो
मीर अनीस
वो क़फ़स क्या जो तह-ए-दामन-ए-सय्याद न हो
अनीस की तबियत आज़ादी पसंद थी और अपने ऊपर किसी तरह की बंदिश (पाबंदी) उनको गवारा नहीं थी। एक बार नवाब अमजद अली शाह को ख़्याल आया कि ‘शाहनामा’ की तर्ज़ पर अपने ख़ानदान की एक तारीख़ नज़्म कराई जाए। इसकी ज़िम्मेदारी अनीस को दी गई। अनीस ने पहले तो औपचारिक रूप से मंज़ूर कर लिया, लेकिन जब देखा कि उनको रात-दिन सरकारी इमारत में रहना होगा, तो किसी बहाने से इनकार कर दिया।
आख़िरी पड़ाव और विरासत
जिस तरह अनीस का कलाम जादुई है, उसी तरह उनका पढ़ना भी नायाब था। मिंबर पर पहुंचते ही उनकी शख़्सियत बदल जाती थी। आवाज़ का उतार-चढ़ाव, आंखों की गर्दिश और हाथों की जुंबिश (हरकत) से वो सामईन (सुनने वालों) पर जादू कर देते थे, और लोगों को तन-बदन का होश नहीं रहता था। मर्सिया-ख़्वानी में उनसे बढ़कर माहिर कोई नहीं पैदा हुआ।
आख़िरी उम्र में उन्होंने मर्सिया-ख़्वानी बहुत कम कर दी थी। 1874 ई. में लखनऊ में उनका इंतेकाल हुआ। उन्होंने तक़रीबन 200 मर्सिये और 125 सलाम लिखे। इसके इलावा करीब 600 रुबाईयां भी उनकी यादगार हैं, जो उनके कलाम की वुसअत को ज़ाहिर करती हैं।
तमाम उम्र जो की हम से बे-रुख़ी सब ने
मीर अनीस
कफ़न में हम भी अज़ीज़ों से मुंह छुपा के चले
ये भी पढ़ें: इस्मत चुग़ताई: उर्दू अदब की बुलंद आवाज़ और बेबाक कलम की शख़्सियत
आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं