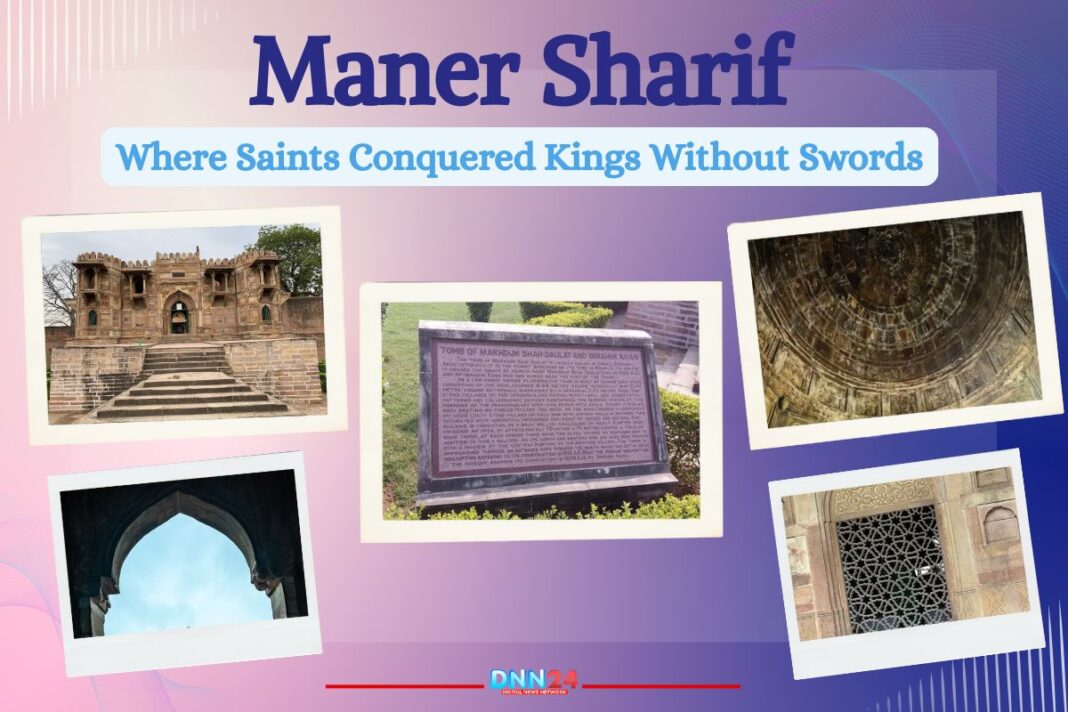उर्दू अदब की तारीख़ में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ़ अपनी इल्मी ख़िदमत की वजह से नहीं, बल्कि अपने अदबी जुनून और दीवानगी की वजह से भी हमेशा याद रखे जाते हैं। उन्हीं रोशन चिराग़ों में एक नाम है मुहम्मद हुसैन आज़ाद।
एक ऐसी शख़्सियत जिसने मुश्किलात, फ़ाक़ों, तन्हाई, दीवानगी और तबाही के दौर में भी वो कारनामे अंजाम दिए जिनकी कल्पना होश-ओ-हवास में भी कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने न सिर्फ़ उर्दू नस्र को एक नया अंदाज़ दिया, बल्कि उर्दू नज़्म को भी नई राह दिखाई। उनका कलम इतना जुनूनी, इतना असरदार था कि उन्होंने आलोचना (क्रिटिसिज्म) की एक नई परंपरा डाल दी। मौज़ूआती मुशायरों की नींव उन्होंने रखी, उर्दू ज़बान की पैदाइश पर नई रोशनी डाली और बृज भाषा को उर्दू का बुनियादी स्रोत साबित किया।
यही नहीं, उन्होंने उर्दू की तरक़्क़ी के लिए अंग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषाओं से सीख लेने पर ज़ोर दिया और उर्दू शायरी के मिज़ाज को गहरी सोच और अशय (थीम) से जोड़ने की राह खोली। उनके अदबी सफ़र का बुलंद नुक्ता है ‘आब-ए-हयात’, एक ऐसी किताब जिसकी वजह से उन्हें उर्दू अदब में अमरता हासिल हो गई। ये सिर्फ़ तज़किरा नहीं, बल्कि उर्दू ज़बान की तामीर और तरक़्क़ी का पहला बड़ा बयान भी है।
दिल्ली में पैदाइश और बचपन
मुहम्मद हुसैन आज़ाद 5 सितंबर 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। ये वो दौर था जब दिल्ली के चमन में तहज़ीब की ख़ुशबू थी, मगर मुल्क का सियासी आसमान काली घटाओं में घिरता जा रहा था। उनके वालिद मौलवी मुहम्मद बाक़िर उत्तरी भारत के पहले उर्दू अख़बार ‘दिल्ली उर्दू अख़बार’ के संपादक थे। उनका अपना प्रिंटिंग प्रेस था, इमामबाड़ा था, मस्जिद थी, सराय थी यानी एक संपन्न और सम्मानजनक घराना था।
मौलवी बाक़र उर्दू के पहले शहीद-ए-सहाफ़त (शहीद पत्रकार) थे। उन्हें अंग्रेज़ अधिकारी मिस्टर टेलर के क़त्ल के इल्ज़ाम में सन् 1857 में फांसी दे दी गयी। आज़ाद की उम्र उस वक़्त महज़ चार साल थी जब उनकी मां का इंतक़ाल हो गया। फ़ूफ़ी ने परवरिश की, लेकिन उनका साया भी जल्द उठ गया। इन दर्दनाक हादसों ने बचपन से ही उनके दिल में एक अजीब किस्म की तड़प, बेचैनी और संजीदगी पैदा कर दी।
दिल्ली कॉलेज की तालीम और तबाह होते हालात
जब वो दिल्ली कॉलेज में तालीम ले रहे थे, मुल्क की फ़िज़ा बिगड़ने लगी। 1857 की जंग ने सब कुछ हिला दिया। उनके वालिद की गिरफ़्तारी के बाद उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। वह कई महीनों तक अलग-अलग जगहों में छिपकर रहते रहे। कभी लखनऊ, कभी किसी रिश्तेदार के यहां। करीब दो-ढाई साल उन्होंने बेइंतहा परेशानियों में गुज़ारे।
इसके बाद वह किसी तरह लाहौर पहुंचे और जनरल पोस्ट ऑफ़िस में छोटी सी नौकरी मिल गयी।
अंजुमन-ए-पंजाब ने खोले नए दरवाज़े
तीन साल बाद उन्हें डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के दफ्तर में नौकरी मिल गयी। उसी दौरान ‘अंजुमन-ए-पंजाब’ की बुनियाद पड़ी और यहीं से उनकी किस्मत चमक उठी।
डॉ. लाइअन्स की कोशिशों से आज़ाद अंजुमन-ए-पंजाब के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। ये वो मंच था जिसने उनकी अदीबी काबिलियत को पहचान दिलाई। (टॉपिक-बेस्ड मुशायरे) की शुरुआत उन्होंने यहीं से की। ये उनकी सबसे बड़ी अदबी इनोवेशन में से एक है।
इसके बाद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी के प्रोफे़सर की तात्कालिक(अर्ज़ी तौर पर) और फिर स्थायी नियुक्ति मिल गयी। एक स्थिर नौकरी ने उनके अन्दर का तूफ़ान थोड़ा कम किया। दिमाग़ को राहत मिली और कलम को उड़ान।
सफ़रनामा, इल्म और तजुर्बे की दास्तान
नौकरी के साथ उन्होंने सफ़र का सिलसिला शुरू किया। मध्य एशिया की यात्रा ने उनके सोचने-समझने की दुनिया को बहुत विस्तार दिया। उन्होंने अपने सफ़रों को क़लमबंद किया और “सैर-ए-ईरान” जैसी ख़ूबसूरत किताब लिखी। जिसमें उन्होंने हाफ़िज़ और सादी के वतन से जुड़ी अपनी मीठी-कड़वी यादों को जोड़ा। उनकी रचनाओं की फेहरिस्त लंबी है:
- सुखंदान-ए-फ़ारस
- क़िस्से-हिंद
- दरबार-ए-अकबरी
- निगारिस्तान-ए-फ़ारस
- सैर-ए-ईरान
- दीवान-ए-ज़ौक
- नैरंगे ख़्याल
पाठ्य पुस्तकों में:
- उर्दू की पहली किताब
- उर्दू की दूसरी किताब
- उर्दू की तीसरी किताब
- क़वायद-ए-उर्दू
इन किताबों ने उर्दू तालीम का नक़्शा ही बदल दिया।
आज़ाद की जो किताब उर्दू अदब में “हमेशा” के लिए दर्ज हो गई, वह है “आब-ए-हयात”
यह कोई साधारण तज़किरा नहीं, बल्कि उर्दू शायरी का पहला मुकम्मल इतिहास है भाषाई तर्कों, तहज़ीबी तफ़सीलों और तख़लीक़ी अंदाज़ के साथ। यह किताब उर्दू आलोचना की नींव भी है। इसमें उन्होंने पुराने तज़किरों के ढर्रे को तोड़ा और नया “नस्र” का अंदाज़ पेश किया। “आब-ए-हयात” अपनी अवधारणा, भाषा और तर्क की वजह से उर्दू अदब में एक इंकलाब की हैसियत रखती है।
आज़ाद- निबंधकार, आलोचक, शोधकर्ता और नज़्म निगार
आज़ाद सिर्फ़ किस्सागो नहीं थे। वह एक बेहतरीन निबंधकार, आलोचक और रिसर्चर भी थे। उन्होंने उर्दू भाषा के इतिहास, इसके विकास और इसके असल स्रोत पर कई अहम शोधपूर्ण लेख लिखे।
सबसे दिलचस्प बात यह कि वह नज़्म के शुरुआती शायरों में से थे। उन्होंने सिर्फ़ नज़्म लिखी ही नहीं, बल्कि नज़्म को नई दिशा दी। उनकी नज़्मों में रूमान नहीं, अफ़कार (विचार) और “उद्देश्य” मिलता है जो उनके दौर में बिल्कुल नया था।
ज़िंदगी का आख़िरी दौर- दर्द, दीवानगी और तन्हाई
जिंदगी के आख़िरी दिन बेहद दर्दनाक थे। उनकी शरीक-ए-हयात का इंतक़ाल हो गया, और आज़ाद पर जुनून और बेचैनी की हालत हावी हो गई। तन्हाई बढ़ती गयी, दिमाग़ी हालत बिगड़ने लगी। आख़िरकार 22 जनवरी 1910 को उनका इंतक़ाल हो गया।
अंग्रेज़ों के साथ रिश्ते की कहानी
याद रखने की बात यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखने से की थी। अपने वालिद के अख़बार में वह खुलकर आलोचना लिखते थे।लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उनके वालिद को फांसी दी और उनकी ज़िंदगी उलट-पुलट हो गयी, उनके विचारों में बदलाव आया।
अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें न सिर्फ़ माफ़ किया बल्कि “शम्स-उल-उलमा” का ख़िताब भी दिया। इस विरोध से वफ़ा का सफ़र उनके जीवन की विडंबना भी है और वास्तविकता भी।
है इम्तिहां सर पर खड़ा, मेहनत करो मेहनत करो
मुहम्मद हुसैन आज़ाद
बांधो कमर बैठे हो क्या, मेहनत करो मेहनत करो
उनके लिखे हुए शेरों और नज़्मों में जो तड़प है, वह उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुनाती है।
मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू अदब को वो पहचान दी, जिसकी वजह से आज उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान नहीं, बल्कि एक तहज़ीब, एक जज़्बा और एक सोच बन गयी है।
ये भी पढ़ें: अब्दुल मन्नान समदी: रूहानी एहसास और अदबी फ़िक्र का संगम
आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारा YouTube चैनल भी सबस्क्राइब कर सकते हैं।